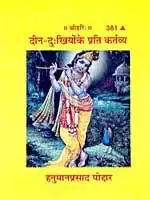|
गीता प्रेस, गोरखपुर >> दीन-दुःखियों के प्रति कर्तव्य दीन-दुःखियों के प्रति कर्तव्यहनुमानप्रसाद पोद्दार
|
264 पाठक हैं |
||||||
इसमें दीन-दुःखियों के प्रति मनुष्य का क्या कर्तव्य है इसका वर्णन किया गया है।
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
भगवान् आर्तिहरण हैं। वे आर्तों की आर्ति हरण करनेवाले हैं। भगवान्
दीनबन्धु हैं, दीनों के सहज मित्र हैं। दीनका अर्थ है—असमर्थ,
अशक्त। जिसमें कुछ भी करने की शक्ति नहीं, जिसके पास कोई साधन नहीं, जो
शक्तिहीन, सामग्रीहीन और सर्वथा निर्बल है—ऐसा जो कोई होता है
उसके
हृदय की पुकार स्वाभाविक ही दीनबन्धु के लिये होती है। दीनको कौन अपनाये ?
संसार में दीनों के साथ सहज, सरल प्रेम करने वाले उनका समादर करने वाले,
उन्हें अपनाने वाले वस्तुतः दो ही हैं—एक भगवान् और दूसरे संत।
यह
दीनबन्धुत्व, दीनवत्सलता, अकिञ्चनप्रियता, दीनप्रियता भगवान् और संत में
ही है। यह परम आदर्श गुण है।
इसका यदि किसी के जीवनमें समावेश हो जाय तो उसका जीवन धन्य हो जाय। इसमें एक विशेष बात यह है जैसे माता संतानवत्सला होती है और वह अपने मन में कभी भी अहंकार नहीं करती कि मैं संतान का उपकार करती हूँ, उसका वात्सल्य उसे संतान की सेवा करने के लिए बाध्य करता है। इस मातृवात्सल्यपर संतान का सहज अधिकार है। माता की वह वत्सलता संतान की सम्पत्ति है। उसकी वह वत्सलता संतान के लिये ही है, नहीं तो उसकी कोई सार्थकता नहीं। इसी प्रकार दीनों के प्रति अनाथों के प्रति, दुःखियों के प्रति जो संतों की, भगवान् की सहज दयापूर्ण वत्सलता है, वह अनाथों, अनाश्रितों, दीनों, दुःखियों और असहायों की निज सम्पत्ति है।
दीनों के प्रति सहज वत्सलता रखनेवाले पुरुषों का यह स्वभाव होता है। यह सहज भाव सदा उनके हृदय में रहता है। वे यह नहीं मानते कि हम किसी का उपकार कर रहे हैं। वे नहीं मानते कि हम दया करके किसी ‘दीन’—दया के पात्र को कुछ दे रहे हैं। वे अपना कुछ मानते ही नहीं। वे समझते है हमारा कुछ है ही नहीं। जो कुछ है सब भगवान् का है। विद्या, बुद्धि, बल, धन, सम्पत्ति, जमीन, मकान जो कुछ है, सारा-का-सारा भगवान् का है। इसलिये उसको यथायोग्य निरन्तर भगवान् की सेवा में-भगवान् के काममें लगाते रहना, यह उनका स्वभाव होता है।
अतः उनकी दीनवत्सलता, किसी दीनका उपकार नहीं, भगवान्की सेवा है। भगवान् की अपनी वस्तु, भगवान् को समर्पण करने का भाव है। इस भाव के विपरीत जो उन सब वस्तुओं का संग्रह करता है, जो उन्हें अपनी वस्तु मानता है, उनपर अपना स्वामित्व, अपना अधिकार मानता है, भगवान् की अपनी वस्तु भगवान् को देता नहीं, वह चोर है, भगवान् की चीजपर अपना स्वत्व मानकर जो सब कुछ को अपना मान बैठता है, केवल अपने ही उपयोग में लेने लगता है वह चोर है, दण्डका पात्र है। श्रीमद्भागवत में देवर्षि नारदजी ने कहा है—
इसका यदि किसी के जीवनमें समावेश हो जाय तो उसका जीवन धन्य हो जाय। इसमें एक विशेष बात यह है जैसे माता संतानवत्सला होती है और वह अपने मन में कभी भी अहंकार नहीं करती कि मैं संतान का उपकार करती हूँ, उसका वात्सल्य उसे संतान की सेवा करने के लिए बाध्य करता है। इस मातृवात्सल्यपर संतान का सहज अधिकार है। माता की वह वत्सलता संतान की सम्पत्ति है। उसकी वह वत्सलता संतान के लिये ही है, नहीं तो उसकी कोई सार्थकता नहीं। इसी प्रकार दीनों के प्रति अनाथों के प्रति, दुःखियों के प्रति जो संतों की, भगवान् की सहज दयापूर्ण वत्सलता है, वह अनाथों, अनाश्रितों, दीनों, दुःखियों और असहायों की निज सम्पत्ति है।
दीनों के प्रति सहज वत्सलता रखनेवाले पुरुषों का यह स्वभाव होता है। यह सहज भाव सदा उनके हृदय में रहता है। वे यह नहीं मानते कि हम किसी का उपकार कर रहे हैं। वे नहीं मानते कि हम दया करके किसी ‘दीन’—दया के पात्र को कुछ दे रहे हैं। वे अपना कुछ मानते ही नहीं। वे समझते है हमारा कुछ है ही नहीं। जो कुछ है सब भगवान् का है। विद्या, बुद्धि, बल, धन, सम्पत्ति, जमीन, मकान जो कुछ है, सारा-का-सारा भगवान् का है। इसलिये उसको यथायोग्य निरन्तर भगवान् की सेवा में-भगवान् के काममें लगाते रहना, यह उनका स्वभाव होता है।
अतः उनकी दीनवत्सलता, किसी दीनका उपकार नहीं, भगवान्की सेवा है। भगवान् की अपनी वस्तु, भगवान् को समर्पण करने का भाव है। इस भाव के विपरीत जो उन सब वस्तुओं का संग्रह करता है, जो उन्हें अपनी वस्तु मानता है, उनपर अपना स्वामित्व, अपना अधिकार मानता है, भगवान् की अपनी वस्तु भगवान् को देता नहीं, वह चोर है, भगवान् की चीजपर अपना स्वत्व मानकर जो सब कुछ को अपना मान बैठता है, केवल अपने ही उपयोग में लेने लगता है वह चोर है, दण्डका पात्र है। श्रीमद्भागवत में देवर्षि नारदजी ने कहा है—
यावद् भ्रियेत जठरं तावत् स्वत्वं हि देहिनाम्।
अधिकं योऽभिमन्येत स स्तेनो दण्डमर्हति।।
अधिकं योऽभिमन्येत स स्तेनो दण्डमर्हति।।
(7/14/8)
‘‘जितने से पेट भरे—सादगी से जीवन-निर्वाह
हो, उतने पर
ही अधिकार है। जो उससे अधिकपर अपना अधिकार मानता है, संग्रह करता है, वह
दूसरों के धन पर अधिकार मानने वाले की तरह चोर है और दण्ड का पात्र है।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book